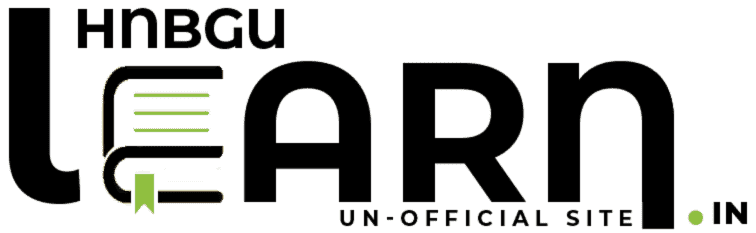ज्वार-भाटा
Table of Contents
ज्वार-भाटा क्या हैं, इनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालें।
सूर्य तथा चन्द्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है और इससे उत्पन्न तरंगों को ‘ज्वारीय तरंग’ कहते है। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ‘ज्वार’ (Tide) तथा उस समय निर्मित उच्च जलतल को उच्च ज्वार (High Tide) तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर (सागर की ओर) पीछे लौटने को भाटा तथा उसमें निर्मित निम्न जल को निम्न ज्वार (Low Tide) कहते हैं।
विभिन्न स्थानों पर ज्वार-भाटा की ऊँचाई में पर्याप्त भिन्नता होती है। यह भिन्नता सागर में जल की गहराई, सागरीय तट की रूप-रेखा तथा सागर के खुले होने या बन्द होने पर आधारित होती है।
ज्वार की उत्पत्ति
पृथ्वी के महासागरीय जल में ज्वार की उत्पत्ति चन्द्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बलों द्वारा होती है। चन्द्रमा का केन्द्र पृथ्वी के केन्द्र से 3,84,800 किमी. दूर है तथा पृथ्वी की सतह चन्द्रमा की सतह से 3,77,600 किमी. दूर है। स्पष्ट है कि चन्द्रमा के सामने पृथ्वी की सतह वाले भाग के पीछे स्थित भाग चन्द्रमा की सतह से 3,90,400 किमी दूर स्थित होगा। अतः चन्द्रमा के सामने स्थित भाग पर चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव होता है तथा उसके पीछे स्थित भाग पर न्यूनतम। परिणामस्वरूप चन्द्रमा के सामने स्थित पृथ्वी के भाग का जल ऊपर खिंच जाता है, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। इस कारण 24 घण्टे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार तथा दो भार भाटा आता है।
जब सूर्य तथा चन्द्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, तो दोनों की आकर्षण शक्ति मिलकर एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य तथा चन्द्रमा के आकर्षण बल एक-दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार अनुभव किया जाता है। यह स्थिति प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है।
ज्वार का समय
प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में दो बार ज्वार आता है। चूंकि पृथ्वी 24 घण्टे में अपनी धुरी पर एक पूर्ण चक्कर लगा लेती है, अतः प्रत्येक स्थान पर 12 घण्टे के बाद ज्वार आना चाहिये। अर्थात् प्रत्येक दिन ज्वार एक ही समाय पर आना चाहिये, परन्तु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रतिदिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। इसका प्रमुख कारण चन्द्रमा का भी अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुये पृथ्वी की परिक्रमा करना है।
ज्वार के प्रकार
ज्वार को कई प्रकारों में विभक्त किया जाता है। ज्वार के कुछ प्रमुख प्रकार निम्न
हैं —
पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार
जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा एक सरल रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को युति-वियुति या सिजिगी (Syzygy) कहते हैं। इनमें से जब सूर्य, चन्द्रमा तथा पृथ्वी क्रम से एक सीध में होते हैं, अर्थात् सूर्य तथा चन्द्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, तो उसे युति (सूर्यग्रहण की स्थिति) कहते हैं और जब सूर्य तथा चन्द्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं, तो उसे समकोणिक स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या (New Moon) तथा वियुति की स्थिति पूर्णमासी (Full Moon) की होती है। इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में दो बार (अमावस्या तथा पूर्णमासी को) आते है तथा इनका समय निश्चित होता है। दीर्घ ज्वार के समय भाटा की निचाई सर्वाधिक होती है।
अनयवृत्ती ज्वार (tropical tides) और भूमध्यरेखीय ज्वार (equatorial tide)
जब चन्द्रमा का उत्तर की ओर अधिकतम (दूरतम) झुकाव होता है, तो चन्द्रमा की किरणें ज्वार केन्द्र पर लम्बवत् पड़की है, जिस कारण उच्च ज्वार आता है तथा वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर होता है। कर्क रेखा के ज्वार केन्द्र के विपरीत स्थित मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार आता है। इस प्रकार के कर्क तथा मकर रेखाओं के समीप आने वाले क्रमिक ज्वार तथा भाटा (Successive High and Low Tide Waters) असमान ऊँचाई वाले होती हैं। इस तरह के ज्वार-भाटे सामान्य ज्वार-भाटे से क्रमशः अधिक ऊँचे तथा नीचे होते है। परन्तु दूसरे दिन के ज्वार में अन्तर नहीं होता। इस तरह की ज्वार की घटना को दैनिक असमानता (Diurnal Inequality) कहते हैं। यह स्थिति महीने में दो बार होती है, जबकि चन्द्रमा का अधिकतम झुकाव (उत्तरायण-कर्क रेखा के पास तथा दक्षिणायन मकर रेखा के पास की स्थितियों के समय) होता है। इन स्थितियों में कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को अनयवृत्ती ज्वार (Tropical Tides) कहते हैं। हर महीने में चन्द्रमा भूमध्य रेखा पर लम्बवत् होता है, जिस कारण दैनिक असमानता लुप्त हो जाती है, क्योंकि दो उच्च ज्वारों की ऊंचाई तथा दो निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। इसे भूमध्यरेखीय ज्वार (Equatorial Tide) कहते हैं।
लघु ज्वार
प्रत्येक मास के शुक्लपक्ष तथा कृष्णपक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चन्द्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। ये मिलकर समकोण बनाते हैं। उसके फलस्वरूप सूर्य तथा चन्द्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक-दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है। इसे लघु ज्वार कहा जाता है। ज्वार तथा भाटे के जल की ऊँचाई का अन्तर बहुत कम रहता है।
जब चन्द्रमा पृथ्वी की निकटतम (पृथ्वी के केन्द्र से चन्द्रमा के केन्द्र की दूरी 3,56,000 किमी.) होता है, तो उसे चन्द्रमा की उपभूस्थिति (Perigee) कहते हैं। इस स्थिति में चन्द्रमा का जवारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है। जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होता है, इसे उपभू या भूमि नीच ज्वार (Perigean Tide) कहते हैं। इससे विपरीत जब चन्द्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है तो उसे अपभूस्थिति कहते हैं। जब लघु ज्वार (Neap Tide) तथा अपभू ज्वार एक साथ आते हैं तो ज्वार तथा भाटा का जल-तल अत्यन्त कम हो जाता है।
दैनिक ज्वार
किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले ज्वार तथा भाटा को ‘दैनिक ज्वार-भाटा’ कहते हैं। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। इस तरह का ज्वार चन्द्रमा के झुकाव के कारण आता है।
अर्द्ध दैनिक ज्वार
किसी स्थान पर प्रत्येक दिन दो बार आने वाले ज्वार को ‘अर्द्ध दैनिक ज्वार’ कहते है। प्रत्येक ज्वार 12 घण्टे 26 मिनट बाद आता है। यह ज्वार, ज्वार के दो केन्द्रों के कारण आता है। दोनों ज्वारों की ऊँचाई तथा दोनों भाटा की निचाई समान होती है।
मिश्रित ज्वार
किसी स्थान में आने वाले असमान अर्द्धदैनिक ज्वार को ‘मिश्रित ज्वार’ कहते हैं। अर्थात् दिन में दो ज्वार तो आते हैं, परन्तु एक ज्वार की ऊँचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाट की निचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है।
ज्वार-भाटे के प्रभाव
ज्वार-भाटे का प्रभाव नौका-परिवहन पर अत्यधिक पड़ता है। ज्वार द्वारा कुछ नदियाँ बड़े जलयानों के चलने योग्य बन जाती हैं। हुगली तथा टेम्स नदियाँ ज्वारीय धाराओं के कारण ही नाव्य हो सकी हैं तथा कोलकाता व लन्दन महत्त्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। ज्वारीय ऊर्जा को भी आज महत्त्वपूर्ण समझा जाने लगा है। ज्वार के द्वारा समुद्रतटीय नगरों के कूड़े व गन्दगी के ढेर बहकर समुद्र में चले जाते हैं।
- e.knowledge_shahi
Related Topics
Share